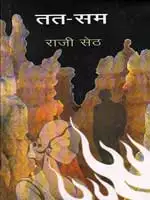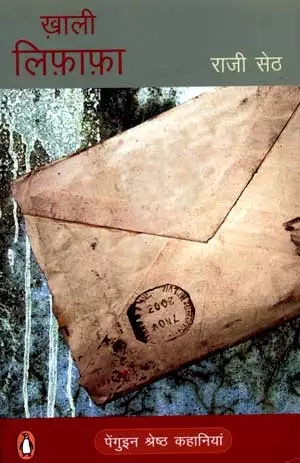|
उपन्यास >> तत सम तत समराजी सेठ
|
78 पाठक हैं |
|||||||
अपने पात्रों की नियति को तत-समता के अभिशाप से उबारकर लाता यह उपन्यास जिजीविषा के मर्म-भेदन का आलोकपर्व है।
Tat-Sum - A Hindi Book - by Raji Seth
कैसे क्या होगा, मेरी चिन्ता थी। इस चीथड़े-चीथड़े मन को तुम्हारे सामने ले जाकर क्या करूँगा ? क्या कहूँगा—मैं वह नहीं, जो कल था ? मैं उसका भूत हूँ...मैं उसकी छाया—गूँगी और अवरूद्ध ? सहस्त्रों किरचों के बीच खील-खील खंडित हो गया था वह स्वीकार जिसे मेरी दृष्टि में एक साबुत स्वीकार होना था। पूरी सहमति, पूरी प्रफुल्लता के साथ। उस समय तो मैं और भी आविष्ट था अतीत में। इच्छा से नहीं, जकड़न से। वह तो और भी अनुपयुक्त घड़ी थी—अधूरी। तुम्हारे प्रति प्रीति से नहीं, अपनी मुक्ति की इच्छा से आच्छादित। तब प्राथमिक लगी थी मुझे अपनी पात्रता की बात। जो बोया था, उसे काटना जरूरी था। नए बीज डालने के लिए धरती को खाली कर लेना पड़ता है।
तुम्हें कहना तो चाहता था—वसुधा, प्रतीक्षा करो...मेरी प्रतीक्षा करो...बियर विद मी...स्टैंड बाइ माई साइड जब तक कि हालाँकि यह ‘जब तक’ कितनी लम्बी होगी, कितनी तावील, इसका मुझे कोई एहसास नहीं। यों भी कैसे मेरा हो गया तुम्हारे उदार प्रीति भाव को बन्धक रखने का अधिकार किस आधार पर, जबकि जानता था, तुम स्वयं एक जमीन ढूँढ़ती काँपती हुई अस्मिता हो ?
‘वह भी तो वहीं खड़ी थी, उसी पड़ाव पर—
अतीत अभाव में
वर्तमान रिक्तभाव में
भविष्य अनिश्चित
उसकी भी वैसी ही थी यात्रा
उसके समान–तत-सम...’
अपने पात्रों की नियति को तत-समता के इस अभिशाप से उबारकर लाता यह उपन्यास जिजीविषा के मर्म-भेदन का आलोकपर्व है। यहाँ दुख दुख नहीं, दृष्टि है—कुछ ऐसी प्राणवत्ता का उपार्जन, जो ‘गिर जाने पर कपड़े झाड़कर खड़े हो जाने का संकल्प और आत्मबल भी देता है’—फिर भी यह कोई प्रेमकथा नहीं है, न स्त्री-विमर्श की दिशा में चिन्तन के हाथ बढ़ाने की कोई आवेगित कोशिश। यहाँ नियतिबद्ध मनुष्यों को अपने चैतन्य की तलाश है जहाँ अपने को अपनी समग्रता में पाने के लिए उनकी आन्तरिकता भरपूर कदम उठाना चाहे, क्योंकि यहाँ शत्रु समाज या स्थिति नहीं, अपनी जड़ता है। जिजीविषा के उत्सव का यह दस्तावेज सदा अर्थजीवी रहेगा, इसमें सन्देह नहीं।
यह उपन्यास और भी कई अर्थों में अपूर्व है। इसकी संरचना घटनाओं से नहीं, मनःस्थितियों से हुई है—कथा-विन्यास को कपड़े के अस्तर की तरह खोलते हुए। भाषा यहाँ अभिव्यक्ति का उपकरण नहीं, शुद्ध संवेदन है—स्थिति की अनुकूलता में पूरी तरह विगलित, स्पन्दित। पाठ की सघन बुनावट हर बार नए से नया अर्थ देने में सक्षम। शैली-शिल्प की ऐसी प्रस्तुति और ऐसी जीवन-दृष्टि उस दशक के उपन्यासों में विरल रही है।
तुम्हें कहना तो चाहता था—वसुधा, प्रतीक्षा करो...मेरी प्रतीक्षा करो...बियर विद मी...स्टैंड बाइ माई साइड जब तक कि हालाँकि यह ‘जब तक’ कितनी लम्बी होगी, कितनी तावील, इसका मुझे कोई एहसास नहीं। यों भी कैसे मेरा हो गया तुम्हारे उदार प्रीति भाव को बन्धक रखने का अधिकार किस आधार पर, जबकि जानता था, तुम स्वयं एक जमीन ढूँढ़ती काँपती हुई अस्मिता हो ?
‘वह भी तो वहीं खड़ी थी, उसी पड़ाव पर—
अतीत अभाव में
वर्तमान रिक्तभाव में
भविष्य अनिश्चित
उसकी भी वैसी ही थी यात्रा
उसके समान–तत-सम...’
अपने पात्रों की नियति को तत-समता के इस अभिशाप से उबारकर लाता यह उपन्यास जिजीविषा के मर्म-भेदन का आलोकपर्व है। यहाँ दुख दुख नहीं, दृष्टि है—कुछ ऐसी प्राणवत्ता का उपार्जन, जो ‘गिर जाने पर कपड़े झाड़कर खड़े हो जाने का संकल्प और आत्मबल भी देता है’—फिर भी यह कोई प्रेमकथा नहीं है, न स्त्री-विमर्श की दिशा में चिन्तन के हाथ बढ़ाने की कोई आवेगित कोशिश। यहाँ नियतिबद्ध मनुष्यों को अपने चैतन्य की तलाश है जहाँ अपने को अपनी समग्रता में पाने के लिए उनकी आन्तरिकता भरपूर कदम उठाना चाहे, क्योंकि यहाँ शत्रु समाज या स्थिति नहीं, अपनी जड़ता है। जिजीविषा के उत्सव का यह दस्तावेज सदा अर्थजीवी रहेगा, इसमें सन्देह नहीं।
यह उपन्यास और भी कई अर्थों में अपूर्व है। इसकी संरचना घटनाओं से नहीं, मनःस्थितियों से हुई है—कथा-विन्यास को कपड़े के अस्तर की तरह खोलते हुए। भाषा यहाँ अभिव्यक्ति का उपकरण नहीं, शुद्ध संवेदन है—स्थिति की अनुकूलता में पूरी तरह विगलित, स्पन्दित। पाठ की सघन बुनावट हर बार नए से नया अर्थ देने में सक्षम। शैली-शिल्प की ऐसी प्रस्तुति और ऐसी जीवन-दृष्टि उस दशक के उपन्यासों में विरल रही है।
तत-सम
भीड़ इतनी है परिचय एक भी नहीं।
समारोह का उद्घाटन दोपहर के खाने के बाद तीन बजे होगा। सुबह एकदम खाली-लटकी हुई। अकेलापन फट गये पल्लू की तरह पीछे लिथड़ता हुआ।
डॉ. ललितचन्द्र अपने किसी सम्बन्धी के यहाँ खाली सुबह भुनाने डिर्फेंस कॉलोनी चले गये हैं। लड़कियाँ मग्न हैं अपने में। रिहर्सल के दौरान इतनी पारस्परिक आत्मीयता अर्जित ज़रूर हो गयी है कि अपरिचय के मरु में वह उस टोली में निःशंक बैठ सके, पर वे सब उखड़ी रहती हैं उसके बीच में बैठे होने से। परदा चाहे झील है पर स्वच्छन्दता उस भाव—मैडम के बीच में बैठे होने पर—मिलती भी हो तो अखरती तो ज़रूर है।
समझते हुए नासमझी का प्रदर्शन और भी फूहड़ लगता है।
हर किसी की आँख में खोज है जैसे कुछ भी खोया हुआ इस मेले में मिल जाने को है। नये परिचयों की उछाह। पुराने परिचयों की टटोल। यहाँ-वहाँ बिखरे हुए झुंड। उठते और डूबते ठहाके।
अच्छा ही हुआ उसे बत्रा मिल गया—किशोर बत्रा। अपना सहपाठी। तोंदल हो गया है। पूरी तरह गृहस्थ। पहिचानने में ज़रा-सी देर लगती यदि कान के नीचे वह बड़ा काला निशान देखने में न आ जाता।
‘‘अरे...मिस आनन्द। क्या कहकर बुलाऊँ तुम्हें ? अब क्यों रही होगी आनन्द। तुमने कार्ड तो भेजा नहीं था। कहाँ हो आजकल ?’’ ऐसी अकृत्रिम उत्फुल्लता जाने कितने दिनों बाद देखी है।
‘‘लखनऊ में।’’
‘‘किस कॉलेज में ?’’
‘‘नहीं। यूनिवर्सिटी में।’’
‘‘ठाठ हैं। कब से हो वहाँ ?’’
‘‘चार साल होने आये।’’
‘‘तुमने तो शायद रजिस्ट्रेशन कराया था न रिसर्च के लिए...नहीं ?’’
‘‘हा...! तब ?’’ जैसे वह किसी दूसरे के जीवन खंड का कोई टुकड़ा हो और काटकर सामने रख दिया गया हो। ‘‘तब इरादा किया था फिर छोड़ दिया।’’
‘‘क्यों ? शादी हो गयी ? टिपिकल। सत्तर फीसदी औरतों का यही कहना होता है। जैसे ज़िन्दगी का असली काम पूरा...’’
‘‘अब रिसर्च कर रही हूँ, पूरी होने आयी।’’
‘‘अच्छा ! क्यों ? घर-गृहस्थी से जी ऊब गया ?’’ वह खुलकर हँसने लगा।
‘‘न हीं !’’
‘‘और सुनाओ !’’
‘‘बस ! ठीक है सब...!’’
‘‘ओऽऽहो ! तुम्हारी वही ‘बस’। तुम तो ज़रा भी न में हीं बदलीं। एस.के. की याद हैं ? कहा करता था तुम्हारे मुँह चम्मच डालकर निकलवाने पड़ते हैं शब्द।’’
भीतर कुछ तप गया। एस. के. का स्मरण—दीक्षान्त समारोह का दिन। वह उसके हाथ की मुड़ी-तुड़ी नीले काग़ज़ की गीली चिट्ठी। चेहरे पर आते और जाते रंग। उससे तो यह भी पूछा नहीं जा सका कि वह इतना काँप क्यों रहा है ?
काँपता कौन था उन दिनों इस तरह। सब अकड़ते थे। फब्तियाँ कसते थे। झाड़ियों से लगकर सिगरेट फूँकते खड़े रहते थे। और जान-बूझकर रास्ता काटते अपने को जता जाया करते थे। क्लास शुरू होने से पहले उनकी बेंचों पर डटे मिलते थे। उस सारे हुल्लड़ के रहते क्लास में पहले जाकर बैठने का भी संकट। सब लड़कियाँ दरवाज़े के पास खड़ी रहती थीं—एकजुट। प्रोफेसर के कक्षा में घुसने के साथ अन्दर घुसती थीं।
एस. के. ने चिट्ठी में अपना पता लिखा था। सम्पर्क करने की याचना की थी। गम्भीरता से सोचने के लिए कहा था। वह उन लोगों में से नहीं था जो लकड़ी के डंडे पर प्रेम की पताका बनाकर सामनेवाले के दरवाज़े पर गाड़ आयें। उससे तो कभी कुछ कहा तक नहीं गया था। वह सिर्फ प्रतीक्षा करता रहा था। आजमाता रहा था कि क्या यह सच है कि प्रेम एकांगी नहीं होता। एक के मन में ऐसी ठाठें मारता है तो दूसरे को भी कभी-न-कभी तो ज़रूर भिगोयेगा। अब...आखिर वह कितनी प्रतीक्षा करे। कहाँ तक आजमाये। यूनिवर्सिटी छोड़ने का समय आ गया। वह चली जायेगी। वह भी पता नहीं कहाँ जायेगा...क्या करेगा। फिलहाल आई. ए.एस. में बैठने की तैयारी करना है। और किसी से तो नहीं, उससे तो वह ज़रूर कह सकता है कि अपने सफल हो सकने का उसे पूरा विश्वास है। वह उसके साथ सुखी रह सकेगी क्योंकि वह उसे सुखी रखना चाहता है। पूरे संकल्प और इच्छा से कोई कुछ करना चाहता है तो ज़रूर कर लेता है।
‘‘सुना था, वह आई. एफ. एस. में आ गया है।’’ बत्रा ने उस मुद्रा को भंग किया।
‘‘ज़रूर आ गया होगा।’’ जाने कैसे खोये-खोये ही उसने उत्तर दिया।
उसके अपने विवाह के बाद भी कितने दिनों तक उसके और निखिल के बीच आमोद-प्रमोद का विषय बनी रही थी एस. के. की बात !
‘‘फिर क्या हुआ ?’’ उसकी दोनों बाँहों से घिरे घुटनों की चौकी पर अपनी ठोड़ी रखकर निखिल अपने मुँह को उसके सीने के ऊपरी भाग के आमने-सामने कर लेता था। बिलकुल सामने। बिलकुल पास। इतना कि त्वचा का वह छोटा-सा दहकता हुआ घेरा सारी देह से अलग धड़कने-दहकने लगता था।
‘‘होना क्या था...ऐसे कुछ होता है क्या ?’’
‘‘यानी तुमने उस बेचारे की बात पर एक बार भी गौर नहीं किया ?’’
‘‘गौर क्या करना था...कोई सिर-पैर भी तो हो।’’
‘‘बस ! यही तो लड़कियों की बात है। शादी के नाम पर बकरी बन जाती हैं...बैठी हूँ सिर झुकाये ! आओ ! मुझे हलाल करो।’’
‘‘बकरी नहीं, बकरा हलाल किया जाता है। एक तुम्हीं हो जो बकरी हलाल करते हो !’’
आगे फिर वही...तन-मन की फड़फड़ाती कगारों पर आग लग जाया करती थी। ‘‘आजकल तो विदेश में होगा। सुना था किसी लखपति की लड़की से शादी हो गयी है उसकी। हम सबको पूरा विश्वास था कि वह तुम्हें ज़रूर प्रपोज़ करेगा।’’
मन हुआ कि कह दे वह बत्रा से सारी-की-सारी बात। समय की जेब में पड़े आलतू-फालतू काग़ज़ की तरह अब कहीं भी फेंकी जा सकती थी वह बात, पर बत्रा का व्यक्तित्व ?...पता नहीं क्यों कोई आत्मीयता नहीं उपजती थी। कॉलेज के दिनों से ही नहीं। यह बात अलग है कि अपरिचय के इस अथाह में वही सबसे ज़रूरी लग रहा था, इस समय।
‘‘और सुनाओ...क्या करते हैं तुम्हारे हज़रत ?’’
जान रही थी भीतर-ही-भीतर यह प्रश्न आने को है। चलकर आता हुआ दीख जाता है पहले से। किसी भी दिशा में चलना शुरू करे, बात वहीं पर आकर ठहरती है। आदत पड़ गयी है, पड़ जायेगी। उस निरासक्त भाव की भी जिसमें उत्तर देना एकदम आसान हो जाता है।
‘‘नहीं हैं !’’ उसने धीरे से कहा। कहते हुए अपना ही स्वर उसे उस समय निरावेग ठंडा लगा।
‘‘ओऽह !...आयम सॉरी...!’’ कुछ गड़बड़ा गया जैसे हमेशा गड़बड़ा जाता है। इस सिरे से उस सिरे के बीच में बहती सहजता सहमकर चुप हो जाया करती है। अखरता है सदा-ऐसा ही होना। बार-बार, जगह-जगह पर उसी-उसी दृश्य की आवृत्ति होना। सामनेवाले का पहले स्तब्ध होना फिर दया, करुणा, बेचारगी की टोकरी को उसके सिर पर औंधा कर देना।
‘‘क्या हो गया था ?’’ बहुत संजीदा हो गया बत्रा।
‘‘ऐक्सीडेंट। साथ में जो दोस्त था, वह बच गया...कोई ऐसी गहरी चोट तक नहीं आयी।’’
आवाज़ अपनी ही ऐसी लगी जैसे वह उस दोस्त के बच गये होने का दुख प्रकट कर रही है।—‘‘अच्छा है, बच गया। उसके तो दो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं।’’ जल्दी से बोली।
भारी-सी हो गयी बीच की हवा।
‘‘मैं...यों ही...इतनी देर से बक-बक करता जा रहा था...माफ करना।’’ बत्रा ने दूसरी तरफ़ देखते हुए कहा।
‘‘नऽहीं !...कोई बात नहीं ?’’हमेशा की तरह उसने यह भी कह दिया। पर खुल गयी है भीतर। खुल जाना बहुत छोटे बच्चे की उघड़ जानेवाली आँख की तरह होता है—एकाएक। पड़ी हुई पपड़ियों पर दरकी हुई रक्त की लकीर का आक्रोश दीख जाता है—एकदम साफ़ ! अपने को ही।
‘‘तुम कहाँ हो आजकल ?’’ अपनी अभद्रता स्मरण हो आयी। विनयम के एक हीसिरे पर इस तरह बेध्यान खड़े रहना। विनिमय चाहे औपचारिकता का ही क्यों न हो।
‘‘सागर में। जब से यूनिवर्सिटी छोड़ी है, तब से वहीं पर हूँ। अब तो वहीं मकान भी बनवा रहा हूँ।...हो गया फैसला।’’
‘‘किस बात का ?’’
‘‘टिकने का।’’
इतना आसान होता होगा—कितना लम्बा, कितना छोटा होता है अक्सर एक ही रास्ता।
सरिता दौड़ी-दौड़ी आयी। कास्ट्यूमवाले सन्दूक की चाबी माँगने लगी।
‘‘मैं आऊँ ?’’
‘‘नहीं मैडम, हम लोग ठीक कर लेंगे।’’
‘‘चलो न, कैंटीन में चलकर बैठते हैं।’’ बत्रा की आवाज़ में जमी हुई संजीदगी है जो पहलेवाले बत्रा की छवि की तुलना में उसे कुछ अच्छी-सी लग रही है।
‘‘नहीं ! फिर कभी...अभी तो यहीं हैं न पाँच-छह दिन।’’
‘‘कोई खास काम करना है क्या ?’’
काम ? यह घर है क्या जहाँ किसी को काम की, पढ़ाई की, नीद की, थकान की, आड़ मिल जाये। इतने बड़े समारोह के बीच का अकेलापन उघड़ा हुआ है एकदम। असुरक्षित। घर का-सा मैत्रीभाव उसमें अनुपस्थित है। यहाँ का चलन कुछ दूसरा है। कुछ और तरह की बुलाहट है माहौल में—भीतर से बाहर जाने की। समूह में समूह का भाग बन जाने की। यह बात अलग है यह बुलाहट उसे नहीं छूती। रोओं की नोंकी पर पसरती आगे निकल जाती है चुपचाप।
‘‘नहीं ! कोई काम नहीं...चलते हैं।’’
यह भूलना सम्भव नहीं कि बत्रा कहीं और निकल गया तो भीड़ के अथाह में इस अकेले अपरिचयपन का वह करेगी भी क्या...यहाँ दिल्ली में। इस कैम्प में !
चौंध चुभ रही है यहाँ।
अँधेरे की अभ्यस्त आँखों को चुभ रहा है धूप धुला आकाश। विपुल प्रकाश। ऐसे आहत हो रही है जैसे किसी ने सिनेमाघर के ठंडे आत्मतुष्ट अँधेरे में बेहद सच होते संसार की अटूट विश्वसनीयता में से खींचकर उसे दोपहर की धूप की बेदर्दी के हवाले कर दिया हो।
कैसे भूल गयी थी जीवन का कोई दूसरा चेहरा भी है। उष्णाया हुआ। आत्मीय ! आमन्त्रक। अपने सुख-दुख से आगे भी हस्ती है इस संसार की। खुलकर साँस लेती हुई, खिलखिलाती हुई।
चलना बत्रा के साथ हो रहा है तालकटोरा उद्यान के विराट प्रांगण को तिरछे शार्टकट में काटते हुए। तम्बुओं के अनगिनत जमघट को पीछो छोड़ते हुए। लाल मिट्टी बिछे रास्तों पर चलते हुए। प्रवेशद्वार से प्रांगण के रास्ते के दोनों ओर फहराती रंग-बिरंगी पताकाएँ, जिन पर अलग-अलग विश्वविद्यालयों के प्रतीक-चिन्ह छपे हैं, दायीं ओर छूट गयी हैं; और पूरे विस्तार में दूर-सुदूर तक गये आलोक-स्तम्भों की कतारें बायीं ओर।
अद्भुत है इस अन्तर्विश्वविद्यालीय युवा समारोह का जुटाव। चहल-पहल का हिलता-डुलता अथाह। उत्साह। उमंग। गति। शोर ! सिमट गयी लगती हैं शिष्यों और शिक्षकों के बीच की दूरियाँ। चूर-चूर हो गयी लगती है एकरसता। लगता है एक बड़ा सा परिवार हँसने-खेलने के लिए यहाँ आ जुटा है।
किसी दूसरी तरह की लय में सधा है माहौल। हवा में एक आमन्त्रण है, एक माँग—आत्म-विसर्जन की। अपने भीतर का सबकुछ दे डालने की। भीतर से बाहर लौट पड़ने की। अपने आपको खाली कर देने की।
समारोह का उद्घाटन दोपहर के खाने के बाद तीन बजे होगा। सुबह एकदम खाली-लटकी हुई। अकेलापन फट गये पल्लू की तरह पीछे लिथड़ता हुआ।
डॉ. ललितचन्द्र अपने किसी सम्बन्धी के यहाँ खाली सुबह भुनाने डिर्फेंस कॉलोनी चले गये हैं। लड़कियाँ मग्न हैं अपने में। रिहर्सल के दौरान इतनी पारस्परिक आत्मीयता अर्जित ज़रूर हो गयी है कि अपरिचय के मरु में वह उस टोली में निःशंक बैठ सके, पर वे सब उखड़ी रहती हैं उसके बीच में बैठे होने से। परदा चाहे झील है पर स्वच्छन्दता उस भाव—मैडम के बीच में बैठे होने पर—मिलती भी हो तो अखरती तो ज़रूर है।
समझते हुए नासमझी का प्रदर्शन और भी फूहड़ लगता है।
हर किसी की आँख में खोज है जैसे कुछ भी खोया हुआ इस मेले में मिल जाने को है। नये परिचयों की उछाह। पुराने परिचयों की टटोल। यहाँ-वहाँ बिखरे हुए झुंड। उठते और डूबते ठहाके।
अच्छा ही हुआ उसे बत्रा मिल गया—किशोर बत्रा। अपना सहपाठी। तोंदल हो गया है। पूरी तरह गृहस्थ। पहिचानने में ज़रा-सी देर लगती यदि कान के नीचे वह बड़ा काला निशान देखने में न आ जाता।
‘‘अरे...मिस आनन्द। क्या कहकर बुलाऊँ तुम्हें ? अब क्यों रही होगी आनन्द। तुमने कार्ड तो भेजा नहीं था। कहाँ हो आजकल ?’’ ऐसी अकृत्रिम उत्फुल्लता जाने कितने दिनों बाद देखी है।
‘‘लखनऊ में।’’
‘‘किस कॉलेज में ?’’
‘‘नहीं। यूनिवर्सिटी में।’’
‘‘ठाठ हैं। कब से हो वहाँ ?’’
‘‘चार साल होने आये।’’
‘‘तुमने तो शायद रजिस्ट्रेशन कराया था न रिसर्च के लिए...नहीं ?’’
‘‘हा...! तब ?’’ जैसे वह किसी दूसरे के जीवन खंड का कोई टुकड़ा हो और काटकर सामने रख दिया गया हो। ‘‘तब इरादा किया था फिर छोड़ दिया।’’
‘‘क्यों ? शादी हो गयी ? टिपिकल। सत्तर फीसदी औरतों का यही कहना होता है। जैसे ज़िन्दगी का असली काम पूरा...’’
‘‘अब रिसर्च कर रही हूँ, पूरी होने आयी।’’
‘‘अच्छा ! क्यों ? घर-गृहस्थी से जी ऊब गया ?’’ वह खुलकर हँसने लगा।
‘‘न हीं !’’
‘‘और सुनाओ !’’
‘‘बस ! ठीक है सब...!’’
‘‘ओऽऽहो ! तुम्हारी वही ‘बस’। तुम तो ज़रा भी न में हीं बदलीं। एस.के. की याद हैं ? कहा करता था तुम्हारे मुँह चम्मच डालकर निकलवाने पड़ते हैं शब्द।’’
भीतर कुछ तप गया। एस. के. का स्मरण—दीक्षान्त समारोह का दिन। वह उसके हाथ की मुड़ी-तुड़ी नीले काग़ज़ की गीली चिट्ठी। चेहरे पर आते और जाते रंग। उससे तो यह भी पूछा नहीं जा सका कि वह इतना काँप क्यों रहा है ?
काँपता कौन था उन दिनों इस तरह। सब अकड़ते थे। फब्तियाँ कसते थे। झाड़ियों से लगकर सिगरेट फूँकते खड़े रहते थे। और जान-बूझकर रास्ता काटते अपने को जता जाया करते थे। क्लास शुरू होने से पहले उनकी बेंचों पर डटे मिलते थे। उस सारे हुल्लड़ के रहते क्लास में पहले जाकर बैठने का भी संकट। सब लड़कियाँ दरवाज़े के पास खड़ी रहती थीं—एकजुट। प्रोफेसर के कक्षा में घुसने के साथ अन्दर घुसती थीं।
एस. के. ने चिट्ठी में अपना पता लिखा था। सम्पर्क करने की याचना की थी। गम्भीरता से सोचने के लिए कहा था। वह उन लोगों में से नहीं था जो लकड़ी के डंडे पर प्रेम की पताका बनाकर सामनेवाले के दरवाज़े पर गाड़ आयें। उससे तो कभी कुछ कहा तक नहीं गया था। वह सिर्फ प्रतीक्षा करता रहा था। आजमाता रहा था कि क्या यह सच है कि प्रेम एकांगी नहीं होता। एक के मन में ऐसी ठाठें मारता है तो दूसरे को भी कभी-न-कभी तो ज़रूर भिगोयेगा। अब...आखिर वह कितनी प्रतीक्षा करे। कहाँ तक आजमाये। यूनिवर्सिटी छोड़ने का समय आ गया। वह चली जायेगी। वह भी पता नहीं कहाँ जायेगा...क्या करेगा। फिलहाल आई. ए.एस. में बैठने की तैयारी करना है। और किसी से तो नहीं, उससे तो वह ज़रूर कह सकता है कि अपने सफल हो सकने का उसे पूरा विश्वास है। वह उसके साथ सुखी रह सकेगी क्योंकि वह उसे सुखी रखना चाहता है। पूरे संकल्प और इच्छा से कोई कुछ करना चाहता है तो ज़रूर कर लेता है।
‘‘सुना था, वह आई. एफ. एस. में आ गया है।’’ बत्रा ने उस मुद्रा को भंग किया।
‘‘ज़रूर आ गया होगा।’’ जाने कैसे खोये-खोये ही उसने उत्तर दिया।
उसके अपने विवाह के बाद भी कितने दिनों तक उसके और निखिल के बीच आमोद-प्रमोद का विषय बनी रही थी एस. के. की बात !
‘‘फिर क्या हुआ ?’’ उसकी दोनों बाँहों से घिरे घुटनों की चौकी पर अपनी ठोड़ी रखकर निखिल अपने मुँह को उसके सीने के ऊपरी भाग के आमने-सामने कर लेता था। बिलकुल सामने। बिलकुल पास। इतना कि त्वचा का वह छोटा-सा दहकता हुआ घेरा सारी देह से अलग धड़कने-दहकने लगता था।
‘‘होना क्या था...ऐसे कुछ होता है क्या ?’’
‘‘यानी तुमने उस बेचारे की बात पर एक बार भी गौर नहीं किया ?’’
‘‘गौर क्या करना था...कोई सिर-पैर भी तो हो।’’
‘‘बस ! यही तो लड़कियों की बात है। शादी के नाम पर बकरी बन जाती हैं...बैठी हूँ सिर झुकाये ! आओ ! मुझे हलाल करो।’’
‘‘बकरी नहीं, बकरा हलाल किया जाता है। एक तुम्हीं हो जो बकरी हलाल करते हो !’’
आगे फिर वही...तन-मन की फड़फड़ाती कगारों पर आग लग जाया करती थी। ‘‘आजकल तो विदेश में होगा। सुना था किसी लखपति की लड़की से शादी हो गयी है उसकी। हम सबको पूरा विश्वास था कि वह तुम्हें ज़रूर प्रपोज़ करेगा।’’
मन हुआ कि कह दे वह बत्रा से सारी-की-सारी बात। समय की जेब में पड़े आलतू-फालतू काग़ज़ की तरह अब कहीं भी फेंकी जा सकती थी वह बात, पर बत्रा का व्यक्तित्व ?...पता नहीं क्यों कोई आत्मीयता नहीं उपजती थी। कॉलेज के दिनों से ही नहीं। यह बात अलग है कि अपरिचय के इस अथाह में वही सबसे ज़रूरी लग रहा था, इस समय।
‘‘और सुनाओ...क्या करते हैं तुम्हारे हज़रत ?’’
जान रही थी भीतर-ही-भीतर यह प्रश्न आने को है। चलकर आता हुआ दीख जाता है पहले से। किसी भी दिशा में चलना शुरू करे, बात वहीं पर आकर ठहरती है। आदत पड़ गयी है, पड़ जायेगी। उस निरासक्त भाव की भी जिसमें उत्तर देना एकदम आसान हो जाता है।
‘‘नहीं हैं !’’ उसने धीरे से कहा। कहते हुए अपना ही स्वर उसे उस समय निरावेग ठंडा लगा।
‘‘ओऽह !...आयम सॉरी...!’’ कुछ गड़बड़ा गया जैसे हमेशा गड़बड़ा जाता है। इस सिरे से उस सिरे के बीच में बहती सहजता सहमकर चुप हो जाया करती है। अखरता है सदा-ऐसा ही होना। बार-बार, जगह-जगह पर उसी-उसी दृश्य की आवृत्ति होना। सामनेवाले का पहले स्तब्ध होना फिर दया, करुणा, बेचारगी की टोकरी को उसके सिर पर औंधा कर देना।
‘‘क्या हो गया था ?’’ बहुत संजीदा हो गया बत्रा।
‘‘ऐक्सीडेंट। साथ में जो दोस्त था, वह बच गया...कोई ऐसी गहरी चोट तक नहीं आयी।’’
आवाज़ अपनी ही ऐसी लगी जैसे वह उस दोस्त के बच गये होने का दुख प्रकट कर रही है।—‘‘अच्छा है, बच गया। उसके तो दो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं।’’ जल्दी से बोली।
भारी-सी हो गयी बीच की हवा।
‘‘मैं...यों ही...इतनी देर से बक-बक करता जा रहा था...माफ करना।’’ बत्रा ने दूसरी तरफ़ देखते हुए कहा।
‘‘नऽहीं !...कोई बात नहीं ?’’हमेशा की तरह उसने यह भी कह दिया। पर खुल गयी है भीतर। खुल जाना बहुत छोटे बच्चे की उघड़ जानेवाली आँख की तरह होता है—एकाएक। पड़ी हुई पपड़ियों पर दरकी हुई रक्त की लकीर का आक्रोश दीख जाता है—एकदम साफ़ ! अपने को ही।
‘‘तुम कहाँ हो आजकल ?’’ अपनी अभद्रता स्मरण हो आयी। विनयम के एक हीसिरे पर इस तरह बेध्यान खड़े रहना। विनिमय चाहे औपचारिकता का ही क्यों न हो।
‘‘सागर में। जब से यूनिवर्सिटी छोड़ी है, तब से वहीं पर हूँ। अब तो वहीं मकान भी बनवा रहा हूँ।...हो गया फैसला।’’
‘‘किस बात का ?’’
‘‘टिकने का।’’
इतना आसान होता होगा—कितना लम्बा, कितना छोटा होता है अक्सर एक ही रास्ता।
सरिता दौड़ी-दौड़ी आयी। कास्ट्यूमवाले सन्दूक की चाबी माँगने लगी।
‘‘मैं आऊँ ?’’
‘‘नहीं मैडम, हम लोग ठीक कर लेंगे।’’
‘‘चलो न, कैंटीन में चलकर बैठते हैं।’’ बत्रा की आवाज़ में जमी हुई संजीदगी है जो पहलेवाले बत्रा की छवि की तुलना में उसे कुछ अच्छी-सी लग रही है।
‘‘नहीं ! फिर कभी...अभी तो यहीं हैं न पाँच-छह दिन।’’
‘‘कोई खास काम करना है क्या ?’’
काम ? यह घर है क्या जहाँ किसी को काम की, पढ़ाई की, नीद की, थकान की, आड़ मिल जाये। इतने बड़े समारोह के बीच का अकेलापन उघड़ा हुआ है एकदम। असुरक्षित। घर का-सा मैत्रीभाव उसमें अनुपस्थित है। यहाँ का चलन कुछ दूसरा है। कुछ और तरह की बुलाहट है माहौल में—भीतर से बाहर जाने की। समूह में समूह का भाग बन जाने की। यह बात अलग है यह बुलाहट उसे नहीं छूती। रोओं की नोंकी पर पसरती आगे निकल जाती है चुपचाप।
‘‘नहीं ! कोई काम नहीं...चलते हैं।’’
यह भूलना सम्भव नहीं कि बत्रा कहीं और निकल गया तो भीड़ के अथाह में इस अकेले अपरिचयपन का वह करेगी भी क्या...यहाँ दिल्ली में। इस कैम्प में !
चौंध चुभ रही है यहाँ।
अँधेरे की अभ्यस्त आँखों को चुभ रहा है धूप धुला आकाश। विपुल प्रकाश। ऐसे आहत हो रही है जैसे किसी ने सिनेमाघर के ठंडे आत्मतुष्ट अँधेरे में बेहद सच होते संसार की अटूट विश्वसनीयता में से खींचकर उसे दोपहर की धूप की बेदर्दी के हवाले कर दिया हो।
कैसे भूल गयी थी जीवन का कोई दूसरा चेहरा भी है। उष्णाया हुआ। आत्मीय ! आमन्त्रक। अपने सुख-दुख से आगे भी हस्ती है इस संसार की। खुलकर साँस लेती हुई, खिलखिलाती हुई।
चलना बत्रा के साथ हो रहा है तालकटोरा उद्यान के विराट प्रांगण को तिरछे शार्टकट में काटते हुए। तम्बुओं के अनगिनत जमघट को पीछो छोड़ते हुए। लाल मिट्टी बिछे रास्तों पर चलते हुए। प्रवेशद्वार से प्रांगण के रास्ते के दोनों ओर फहराती रंग-बिरंगी पताकाएँ, जिन पर अलग-अलग विश्वविद्यालयों के प्रतीक-चिन्ह छपे हैं, दायीं ओर छूट गयी हैं; और पूरे विस्तार में दूर-सुदूर तक गये आलोक-स्तम्भों की कतारें बायीं ओर।
अद्भुत है इस अन्तर्विश्वविद्यालीय युवा समारोह का जुटाव। चहल-पहल का हिलता-डुलता अथाह। उत्साह। उमंग। गति। शोर ! सिमट गयी लगती हैं शिष्यों और शिक्षकों के बीच की दूरियाँ। चूर-चूर हो गयी लगती है एकरसता। लगता है एक बड़ा सा परिवार हँसने-खेलने के लिए यहाँ आ जुटा है।
किसी दूसरी तरह की लय में सधा है माहौल। हवा में एक आमन्त्रण है, एक माँग—आत्म-विसर्जन की। अपने भीतर का सबकुछ दे डालने की। भीतर से बाहर लौट पड़ने की। अपने आपको खाली कर देने की।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i